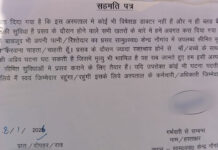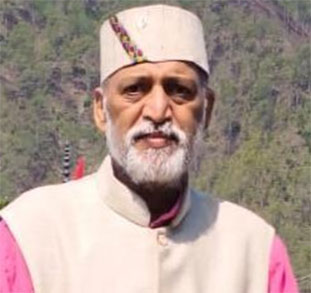
देवेन्द्र कुमार बुडाकोटी
कई साल पुरानी बात है, जब हमारे गाँव का एक आम का पेड़ जिसे हम प्यार से लमथरया कहते थे — अपनी अनोखी मिठास और स्वाद के लिए जाना जाता था — एक तेज बारिश और तूफ़ान नहीं झेल सका और जड़ से उखड़ गया। इस बारे में मुझे मेरे भतीजे की फेसबुक पोस्ट से पता चला।
लेकिन मेरे लिए लमथरया का उखड़ना सिर्फ एक पेड़ का गिरना नहीं था — यह पूरे गाँव के उजड़ने का प्रतीक बन गया।
आख़िर ऐसा कौन-सा तूफ़ान था जिसने गाँव की ज़्यादातर परिवारों को उखाड़ फेंका? यही सवाल मेरे मन में उठता रहा और मुझे गाँव के सामाजिक इतिहास पर विचार करने को मजबूर कर गया। धीरे-धीरे मुझे एहसास हुआ कि हमारा गाँव कोई अपवाद नहीं, बल्कि उत्तराखंड में चल रहे एक बड़े सामाजिक बदलाव का हिस्सा है।
लमथरया की घटना ने मुझे परिवारों के उजड़ने की उस टीस की याद दिला दी। आज की पीढ़ी ने शायद कभी उस आम की मिठास चखी भी नहीं होगी। वे कभी-कभी छुट्टियों में गाँव आ भी जाएँ तो भी उनके लिए लमथरया का गिरना शायद कोई मायने न रखे। लेकिन हमारे लिए — जो गाँव से दूर जा चुके हैं — यह सिर्फ एक पेड़ नहीं, बचपन की यादें, किशोरावस्था के पल, और गाँव के आँगन में बीते जीवन का प्रतीक है।
हमारी पीढ़ी ही वो पीढ़ी है जो नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों में छुपे भावों को समझती है, जो लोकसंगीत के हर सुर में अपनी पहचान देखती है। आज की पीढ़ी के पास शायद गाँव को लेकर कहने-सुनने के लिए ज़्यादा कुछ न हो — लेकिन अगर वे गाँव के सामाजिक इतिहास को जानना चाहें, तो शायद उन्हें भी कुछ जुड़ाव महसूस हो।
उत्तराखंड का सामाजिक इतिहास हमारे गाँव में भी झलकता है। स्वतंत्रता के बाद, कई पहाड़ी परिवारों ने तराई और मैदानी इलाकों में ज़मीन ख़रीदनी शुरू की। द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े पूर्व सैनिकों को 1950 के दशक में सरकार द्वारा ज़मीन दी गई। वे 50 के दशक के अंत में परिवार सहित तराई में बसने लगे, और फिर 60 के दशक में अन्य परिवार भी उनके साथ जुड़ते गए।
70 के दशक में गाँव छोड़ने की प्रक्रिया तेज़ हुई, 80 के दशक में इसमें और गति आई, और 90 के दशक तक यह एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई।
शुरुआती दौर में गाँव से बाहर जाने का “पुल फैक्टर” यानी आकर्षण था — रोज़गार और शिक्षा की बेहतर संभावनाएँ। लेकिन धीरे-धीरे “पुश फैक्टर” यानी मजबूरी हावी हो गई — आजीविका के साधनों की कमी, शिक्षा की ख़राब स्थिति, और कृषि से होने वाली आमदनी का अभाव। राज्य में उद्योग और सेवाक्षेत्र अब भी विकसित नहीं हो पाए हैं।
70 के दशक में पुरुष अपने परिवारों को साथ ले जाने लगे। 80 के दशक में रिटायर हो रहे लोग मैदानों में अपने घर बनवाने लगे। 90 के दशक तक जो सक्षम थे, उन्होंने स्थायी रूप से मैदानों में बसने का निर्णय ले लिया।
60 के दशक तक हमारे जैसे अधिकांश गाँवों में न सड़क थी, न बिजली, न पानी की सुविधा। बच्चे मीलों पैदल चलकर स्कूल जाते थे। कुछ सुविधाएँ 80 और 90 के दशक में आईं, लेकिन तब तक बहुत से परिवार गाँव छोड़ चुके थे या छोड़ने की योजना बना चुके थे।
अब अगर आज जंगली सूअर और बंदरों की समस्या भी हल हो जाए, तब भी खेती दोबारा शुरू नहीं होगी — क्योंकि खेतों के रखवाले ही नहीं बचे हैं।
हमारा चै गाँव इस सामाजिक बदलाव का एक अध्ययन है — ऐसा ही हाल उत्तराखंड के सैकड़ों गाँवों का है। कई गाँव पूरी तरह वीरान हो चुके हैं या हो रहे हैं। परिवार रोज़गार और बच्चों की शिक्षा के लिए नज़दीकी शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं।
राज्य बने दो दशक से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन पहाड़ों में असली विकास और समृद्धि अभी भी दूर की बात लगती है। गाँव अब भी उजड़ रहे हैं, युवा अब भी बाहर जा रहे हैं। 2011 की जनगणना भी इस सच्चाई को आंकड़ों के रूप में सामने रखती है — कि किस तरह पहाड़ों से लोग मैदानों की ओर जा रहे हैं।
मुझे नहीं पता कि योजनाकारों, शिक्षाविदों और विकास विशेषज्ञों के पास पहाड़ों के लिए कोई ठोस योजना है या नहीं। लेकिन मौजूदा हालात को देखकर तो लगता है कि हमारा चै गाँव भी जल्द ही उत्तराखंड के “भूतिया गाँवों” की सूची में शामिल हो जाएगा।
लेखक समाजशास्त्री हैं और चार दशकों से विकास क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनके शोध कार्य का उल्लेख नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन की पुस्तकों में भी किया गया है।