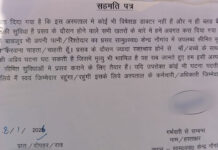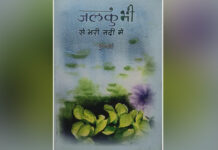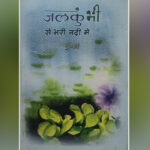देवेंद्र के. बुडाकोटी
भारत में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ छेड़छाड़ और बलात्कार के मामलों में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। इसके साथ ही, विदेशी खुफिया एजेंसियों द्वारा रचे गए “हनी ट्रैप” के ज़रिए ब्लैकमेलिंग की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कई यौन उत्पीड़न के मामलों में अपराधी कोई अनजान व्यक्ति नहीं, बल्कि पीड़िता का करीबी रिश्तेदार या परिचित होता है — अक्सर वही घर, जहां वह खुद को सबसे सुरक्षित मानती है। ऐसे ज्यादातर अपराधों की रिपोर्ट ही नहीं होती।
परिवार सामाजिक बदनामी और लड़की की प्रतिष्ठा या विवाह की संभावनाओं को लेकर डरते हैं और चुप्पी साध लेते हैं। कई बार पीड़िता को सहानुभूति की बजाय दोष और उपहास झेलना पड़ता है। भारत की सख्त नैतिक व्यवस्था, खासकर यौन व्यवहार को लेकर, महिलाओं पर अधिक कठोर होती है। भले ही महिला पीड़िता हो, अपराधी उसे शर्म और डर का हथियार बनाकर ब्लैकमेल करता रहता है।
पीड़िताएं चुपचाप सब कुछ सहती हैं — उन्हें सार्वजनिक अपमान का डर सताता है, और न्याय प्रणाली में विश्वास नहीं होता क्योंकि वह अक्सर धीमी और असंवेदनशील होती है। इस तरह का मानसिक आघात वर्षों तक बना रह सकता है और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।
समाज में प्रचलित यौन नैतिकता ऐसे अपराधों की रिपोर्टिंग को बेहद कठिन बना देती है, खासकर जब अपराधी कोई विश्वस्त पारिवारिक सदस्य या परिचित हो। ऐसे रिश्ते और सामाजिक वर्जनाएं स्थिति को और जटिल बनाते हैं और पीड़िता को पूरी तरह से अलग-थलग कर देते हैं।
“हनी ट्रैप” के मामलों में विदेशी एजेंट उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो संवेदनशील पदों पर होते हैं — जैसे वैज्ञानिक, रक्षा कर्मी या सेना के सदस्य। ये जाल इसलिए प्रभावी हैं क्योंकि समाज में यौन व्यवहार को लेकर गहरी शर्म जुड़ी हुई है। कई बार व्यक्ति को खतरे का एहसास होने के बावजूद, वह सार्वजनिक रूप से उजागर होने के डर और इसके सामाजिक और कानूनी परिणामों के कारण ब्लैकमेल का शिकार बन जाता है।
हालांकि समाज में पूर्व-विवाह और विवाहेतर संबंध मौजूद हैं, फिर भी वे सामाजिक रूप से अस्वीकार्य माने जाते हैं — खासकर महिलाओं के लिए, जिससे वे ब्लैकमेल के लिए अधिक संवेदनशील हो जाती हैं।
ऐतिहासिक रूप से, हनी ट्रैप जासूसी के लिए विश्व युद्धों के समय एक आम रणनीति थी। लेकिन आज कई पश्चिमी देशों में यौनता के प्रति बदलते दृष्टिकोण और प्रगतिशील सामाजिक मानदंडों ने ऐसी रणनीतियों को अप्रभावी बना दिया है। वहां बलात्कार के मामले अधिक रिपोर्ट होते हैं और महिलाओं को उत्तरदायी न्याय प्रणाली तथा जन-जागरूकता से अधिक सुरक्षा मिलती है।
भारत में आज भी नैतिकता, आचार-संहिता और यौन व्यवहार को लेकर गहरे विश्वास कायम हैं। लेकिन यह सख्त नैतिक व्यवस्था न्याय की राह में रोड़ा नहीं बननी चाहिए, और न ही इसे नियंत्रण का हथियार बनाना चाहिए। इसके विपरीत, समाज को पीड़ितों का समर्थन करना चाहिए, न कि उन्हें कलंकित करना।
युवाओं, विशेष रूप से लड़कियों को यह सिखाना जरूरी है कि कैसे परिचित लोग भी शर्म और भावनात्मक नियंत्रण के ज़रिए शोषण कर सकते हैं। बाल यौन शोषण के मामलों में, लड़के और लड़कियों — दोनों को “गुड टच” और “बैड टच” में फर्क सिखाना चाहिए। स्कूलों में दृश्य सामग्री और कार्यशालाएं बच्चों को शोषण को पहचानने और समय रहते बोलने के लिए सक्षम बना सकती हैं।
माता-पिता और शिक्षक इस शिक्षा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें यौन शोषण और ब्लैकमेल की वास्तविकता के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और यह सिखाया जाना चाहिए कि कैसे बिना किसी पूर्वाग्रह के बच्चों का समर्थन किया जाए। ऐसा सुरक्षित और खुला वातावरण बनाना, जहां बच्चे अपनी बात कहने में डरें नहीं, लंबे समय तक चलने वाले मानसिक आघात से बचाने में मदद कर सकता है।
इन समस्याओं का सच में समाधान तभी संभव है जब हम नैतिकता के दिखावे से ऊपर उठकर व्यक्तियों — खासकर महिलाओं और बच्चों — की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। सहमति, सम्मान और सीमाओं पर संवाद शिक्षा और पालन-पोषण का नियमित हिस्सा बनना चाहिए। तभी हम ऐसा समाज बना सकते हैं जहां शर्म पर न्याय की जीत हो, और पीड़ितों को चुप नहीं कराया जाए, बल्कि उनका समर्थन किया जाए।
लेखक एक समाजशास्त्री हैं और 40 वर्षों से अधिक समय तक विकास क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं।